लीलाधर मण्डलोई समकालीन कविता या यूं कहें अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी ,उदय प्रकाश की पीढ़ी के बाद के महत्त्वपूर्ण कवि हैं। अपने प्रारंभिक जीवन और स्कूलिंग के बाद जब मण्डलोई नौकरी में आए और जहां – जहां उनकी पदस्थापनाएं रहीं – लीलाधर मण्डलोई ने वहां की लोकेल्स को अभिव्यक्ति दी। छत्तीसगढ़ का इलाका हो या मध्यप्रदेश का या अंडमान निकोबार का या दिल्ली का – मण्डलोई ने इन स्थानों के जीवन – परिवेश को जीया। इसका सबब यह रहा कि मण्डलोई के कवित्त में जो स्थानीयता थी उसने मण्डलोई को शीर्षस्थानीय कवि के रूप में महत्त्वपूर्ण बनाया। बहरहाल, लीलाधर मण्डलोई ने हाल ही में ‘ जबसे आंख खुली हैं’ आत्मकथा लिखी है। यह आत्मकथा ख़ुद के जीवन के बहाने घर परिवार और उपेक्षित वर्गों की आत्मकथा है। इसमें मण्डलोई के मां बाप भाई बहन मित्र के साथ सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित होकर पहुंचे कोयला खान मज़दूर दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का जीवन है। फ़ाक़ामस्ती भरे जीवन की यह कथा वास्तव में श्रमिक जीवन का शोकगीत है जिसकी अनुगूंज में उल्लास है जो संघर्षशील भारतीय समाज की ख़ासियत है। प्रो. रविरंजन ने इस आत्मकथा पर अपनी दृष्टि भेजी है जो यहां प्रस्तुत है। – हरि भटनागर
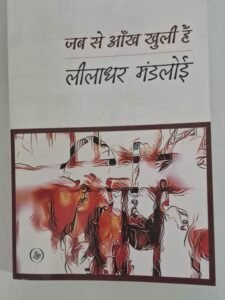
आलेख:
“मैं जिस कबीर समाज से था उसके खिलाफ़ सवर्ण समाज था.गाँव के सरपंच पांडे पिता को हतोत्साहित करते कि बच्चों को न पढ़ाएँ.कक्षा में कभी फ़ारुख़ कभी तो मैं अव्वल होते.उन्हें इससे कोफ़्त होती….मास्टर को बुलाकर कहते कि वे ऊँची जात के बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते…उनका भतीजा जिसे उन्होंने अपने पास बुला लिया था,पढ़ने -लिखने में कमजोर था.स्कूल में सरपंची मुद्रा में रहता.कम नम्बर मिलने पर मास्टरों से झगड़ना और धमकी देना आम बात थी…मेरे प्रति वह बेहद घृणा से भरा हुआ था….अकेले पड़ने पर वह कहता –‘पढ़ाई में अव्वल आता है न एक दिन कहीं घुसेड़ दूंगा.’ जब वह थर्ड डिवीजन में पास होता तो नीच जात कहकर गालियाँ देता…. एक गाली उभरी – ‘… के, ले फर्स्ट आने का फल.’ मेरी बाईं पसली में छुरा घुस चुका था.” (लीलाधर मंडलोई :‘जब से आँख खुली हैं’, पृ.72-74)
साहित्य की एक विधा के रूप में ‘आत्मकथा’ पर विचार करते हुए विलियम सी. स्पेंजेमैन ने ‘द फॉर्म्स ऑफ़ ऑटोबायोग्राफी : एपिसोड्स ऑफ़ हिस्ट्री ऑफ़ लिटरेरी जेनर’ पुस्तक में ‘आत्मकथा’ को ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं काव्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किया है. पूरी दुनिया में ‘आत्मकथा’ के सैद्धांतिक विवेचन के लिए मशहूर इस पुस्तक में लेखक ने अनेक विख्यात यूरोपीय साहित्यिक कृतियों के उदाहरण से यह पुष्ट किया है कि हर तरह का साहित्य कमोबेश आत्मकथात्मक हुआ करता है, लेकिन किसी उपन्यास के किसी पात्र में अगर रचनाकार के व्यक्तित्व का इतना अधिक प्रक्षेपण होने लगता है कि वह आत्मकथा प्रतीत होने लगे,तो ऐसे में लेखकीय विचलन की वजह से उसके लिए ‘आत्मकथा’ शब्द का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता.
‘जब से आँख खुली हैं’ शीर्षक आत्मकथा में लीलाधर मंडलोई ने भी स्वीकार किया है: “ सबसे कठिन होता है बचपन को याद करना.उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है उसे लिखना.लगभग तीस बरस होने को आए और मैं अपनी स्मृतियों को कल्पना से दूर यथार्थ के आंगन में अबेरता, थकता रहा. इसे आत्मकथात्मक उपन्यास के शिल्प में लिख सकता था, लेकिन मुझे लगा मैं जाने-अनजाने अपने बचपन से बेईमानी कर जाऊँगा.”
‘आत्मकथा’ को एक शैली के रूप में परिभाषित करने की कठिनाइयों को स्वीकार करने के बावजूद स्पेंजेमैन इस शब्द को स्वयंसिद्ध मानते हैं. यह सच है कि आत्मकथा की एक अनोखी शैली होती है, पर कुलमिलाकर आत्मकथा समेत सभी कलाकृतियाँ हममें अपने बारे में ऐसी समझ पैदा करती हैं जो अंततः किसी और की नहीं, बल्कि हमारी अपनी होती है।
‘जब से आँख खुली हैं’ से गुज़रते हुए जिस बात का शिद्दत के साथ एहसास होता है वह है रचनाकार की सौन्दर्य-चेतना.बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी के तेज़ाबी यथार्थ का वर्णन-चित्रण करने के क्रम में भी यह सौन्दर्य-चेतना जाग्रत अवस्था में आत्मकथाकार के निजी एवं पारिवारिक जीवन के साथ ही समाज के दबे कुचले लोगों द्वारा भोगी जाने वाली पीड़ा को सर्जनात्मक रूप में पाठक के समक्ष रखती है. याद आ सकते हैं मुक्तिबोध, जिनका कहना है कि ‘सौन्दर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे, संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए….अनुभव-प्रसूत फैन्टेसी में जीवन के अर्थ खोजने और उसमें आनंद लेने की इस प्रक्रिया में ही जो प्रसन्न भावना पैदा होती है, वही एस्थेटिक एक्सपीरिएंस का मर्म है.” स्पष्ट ही सौन्दर्य को वे बुर्जुआ सौन्दर्यशास्त्रियों से विलग अर्थ ग्रहण पर निर्भर मानते हैं जो वस्तुत: संवेदना पर निर्भरता है और संवेदना अंतत: ज्ञान पर निर्भर करती है. चूँकि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार होता है, इसलिए सौन्दर्य सत्य से नाभिनालबद्ध है.
जीवन का सत्य जिस तरह ‘आत्मकथा’ में रूपायित होता है,वैसा अन्य किसी विधा में संभव नहीं है. ऐसे में आत्मकथाकार के सामने सत्य को सम्प्रेषणीय बनाकर पाठकों तक पहुँचाना एक बड़ी चुनौती होती है. ‘जब से आँख खुली हैं’ में आत्मकथाकार लीलाधर मंडलोई ने अपने तईं इस चुनौती का बहुत हद तक सफलता के साथ सामना किया है. इस कृति के आरंभ में आत्मकथा-लेखन को लेकर ऊहापोह के तहत मन में उठनेवाली भाव-तरंगों को उन्होंने एक कविता के माध्यम से व्यक्त किया है:
कुछ बीज हैं स्मृतियों के
कैसी होगी उनकी आमद
उनका अँखुआना कैसा होगा
मैं नहीं जानता
कितनी शक्ति है मानस वसुधा में
याद करते हुए रोशनाई कितना साथ देगी
कितना और कैसा होगा आत्मचरित
सचमुच मैं नहीं जानता
विवेच्य कृति से गुज़रते हुए शिद्दत के साथ महसूस किया जा सकता है कि ‘जब से आँख खुली हैं’ लिखने के लिए मन के गहन गह्वर में उतरकर स्मृतियों को कुरेदते हुए आत्मकथाकार का अपने बचपन में लौटना आसान नहीं रहा है.उसके शब्दों में “लौटने का रास्ता ऊबड़-खाबड़ है…जिस पर नुकीले पत्थड़ हैं बहुत और कांटे.जिन पर माता-पिता नंगे पाँव चले….जंगली रास्ता.पहाड़ की दुर्गमता, भयावह रातें.हिंसक जानवरों का भय…भूख और गरीबी.अकेलापन.इन सबसे विस्थापन के बीच बना एक ऐसा मानस जिसमें लड़ना ही बचा उपाय था.” (पृ.13)
छोटे-बड़े पैंसठ अध्यायों में लिखित विवेच्य कृति में बचपन से लेकर नौकरी पाकर व्यवस्थित और आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित जीवन शुरू करने के पहले तक का विवरण है.इन विवरणों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो दिल दहला देने वाले हैं. बावजूद इसके, जीवन के कटुतम अनुभवों की पुनर्रचना करते वक़्त आत्मकथाकर ने सौन्दर्यबोध का दामन नहीं छोड़ा है. उदाहरण के लिए भयानक अभाव में बीते बचपन का ज़िक्र करते हुए लेखक को माँ द्वारा सुरीले स्वर में गाई जानेवाली एक लोरी याद आती है जिसमें फूलों वाली टोपी का उल्लेख था. इस प्रसंग को याद करते हुए मंडलोई जी लिखते हैं : “दिलचस्प यह था कि न कोई टोपी थी न उसमें फूल.लेकिन लोरी को सुनते हुए लगता था एक टोपी थी.बहुत सुन्दर फूलों वाली.गिरने पर वे बिखर सकते थे. इतनी कोमल और अद्भुत कल्पना.मुझे लगता रहा कि एक टोपी थी ज़रूर.माँ जिसे रखकर भूल गयी या फूलों के गिर जाने के डर से उसने छुपा दी कहीं. वह ढूँढ़ने पर माँ की पेटी में मिल जाएगी…ऐसा आज भी जाने क्यों लगता है …?” (पृ.16)
मंडलोई निरे गद्य लेखक के बजाय सुकवि हैं.इसलिए उनकी आत्मकथा में कुछ ऐसे सूक्ष्म ब्योरे मौजूद हैं जो उन्हें अन्य आत्मकथाकारों से भिन्न एवं विशिष्ट बनाते हैं. इस कृति से गुज़रते हुए पता चलता है कि किसी मजदूर के बच्चे के लिए माता-पिता का एहसास कैसे दूसरे बच्चों से अलहदा होता है:
“माता-पिता मेरे लिए कुछ ध्वनियों से बंधे थे. यानी कुदाल, तसले और फावड़े की ध्वनि. इन्हें जब वे उठाते थे, तो काम पर जाने का बोध होता था और काम से लौटने पर जब पिछवाड़े उन्हें रखते थे तो घर लौट आने का दूसरा ध्वनिबोध.इन वस्तुओं के साथ ध्वनि के स्तर पर हमारा गहरा रिश्ता था…इन ध्वनियों का दूसरा गहरा अर्थ यह भी था कि सब ठीकठाक है…कुछ और ध्वनियाँ हैं जो मन में गहरे तक अंकित हैं.उनमें से एक है बर्तनों की…काँसे के बर्तनों की खनक बहुत रोमांच पैदा करती थी.इसका एक कारण शायद यह भी था कि लोकगीत गाते समय, मैंने माँ को सिक्कों से लोटा बजाते हुए देखा था…माँ की आवाज़ में काँसे की खनक थी.और टनक खरापन था. ” (पृ.17-18)
इस आत्मकथा को पढ़े बगैर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि लेखक का बचपन किन दुश्वारियों को झेलते बीता है:
जबसे आँख खुली हैं अपनी , दर्दो-रंजो-ग़म देखे
इन ही दीद-ए-नमदीदों से क्या-क्या हमने सितम देखे
– मीर
हमलोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन दिनों बालश्रम पर क़ानूनी प्रतिबन्ध के बावजूद अप्रैल –मई की भयावह गर्मी में कोयला खदान में इस्तेमाल होने वाले बायलरों की सँकरी चिमनियों में बच्चों को उतारकर उनसे बायलरों की सफ़ाई का काम करवाया जाता था.अब स्थिति क्या है,यह सर्वेक्षण का विषय है.बचपन को याद करने के क्रम में लेखक ने नवउदारवाद के इस दौर की आलोचना करते हुए लिखा है : “डबलरोटी बाज़ार से ध्वनियों पर चढ़कर आयी पहली चीज़ थी.रोटी के विरुद्ध जिसने घर को घेरा.और अब न केवल उसका ,बल्कि बाज़ारू पैक रोटियों का साम्राज्य है,रोटी के स्वाद पर क़ब्ज़ा करता.नामुराद बाज़ार ने धीरे-धीरे पारंपरिक रोटियों की सुगंध की हत्या करना शुरू कर दिया…अब तरह-तरह के सामिष-निरामिष हॉट डॉग का ज़माना है और बाज़ार की बेसुरी-बेताला ध्वनियाँ” (पृ.20)
लीलाधर मंडलोई द्वारा आत्मकथा लेखन की रचना-प्रक्रिया की टोह लेने की कोशिश के दौरान उनकी जीवनचर्या से मदद मिलती है. उन्होंने उल्लेख किया है कि वे अकेला पड़ जाने पर घर से बाहर निकलने के बजाय लगातार कई दिनों तक आत्मालाप करना पसंद करते हैं.इससे उन्हें अपने भीतर उतरने में मदद मिलती है जो रचनात्मक लेखन के लिए बेहद ज़रूरी है. कहना न होगा कि एक रचनाकार जब अपनी अंतरात्मा को टटोलता है तो उसमें मौन, भय, करुणा, उदासी, क्रोध,घृणा आदि से उसकी मानसिक और संवेदनात्मक मुठभेड़ होती है. इस क्रम में लेखक जागृति का अनुभव करता है और उसकी स्मृति अतीत को खंगालने लगती है.
इस कृति में लेखक के बचपन का झोंपड़ीनुमा घर और उसमें इस्तेमाल किए जानेवाली चीज़ों की जीवंत स्मृति बयान करने के क्रम में जगह जगह कुछेक चित्रण ऐसे हैं जो रचनात्मक कौंध पैदा करने में समर्थ हैं. उदाहरण के लिए मजबूत पत्थर की हाथ- चक्की का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि वह किसी पूर्वज पहाड़ की भारी चट्टान से बिछड़ी हुई है. इसी प्रकार ‘छेनियों की चोटों से होने वाले चक्की के भीतर पाटों के दर्द तक’ न पहुँचने की कसक और चलती हुई चक्की से निष्पन्न संगीत में डूब जाने की इच्छा के बारीक चित्रण से आत्मकथा में जो कवित्व पैदा होता है उसे मूलपाठ से गुज़रे बगैर अनुभव नहीं किया जा सकता.
विवेच्य रचना में माँ और बड़ी बहन का बारम्बार उल्लेख मिलता है और लेखक के जुझारू व्यक्तित्व के निर्माण में इन स्त्रियों की महती भूमिका रही है. इनकी अनेक ख़ूबियों में एक ख़ूबी थी अपनी तकलीफ़ को ख़ुद तक सीमित रखना. माँ के सशरीर न रहने के बावजूद लेखक को उसे याद करने के अनेक कारण हैं जिनमें सबसे प्रमुख है वह ऐन्द्रिय अनुभूति जो ‘माँ के कोमल स्पर्श’ और ‘हथेलियों के पसीने की गंध’ के साथ ही उनके हाथ में पड़े छाले के चलते होने वाले दर्द की अनुभूति को पाठक के भीतर उतार देने की सर्जनात्मक सलाहियत का नमूना हैं. आत्मकथाकार के शब्दों में “माँ कुछ मामले में बेहद स्वार्थी थी.जैसे कि छाले, कष्ट, चुभन, दुःख आदि. इन्हें वह अपने पास ही रखती रही.इन सबका मुसीबतों के साथ उनके पास जैसे एक ख़ज़ाना भरता गया. फिर उसकी चाबी कहीं रखकर वह भूल गयी. न खुद उसे खोलती है न किसी को खोलने की छूट है.उस ख़ज़ाने की एक झिरी, एक दरार है. जो मेरे बचपन में कहीं खुली हुई है.बस एक बेचैनी में वहाँ थोड़ा-सा झाँक आता हूँ.” (पृ.29)
पहले के मुकाबले अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति में सुख-समृद्धि के मद्देनज़र लेखक जब बचपन के दिनों को याद करने के दौरान घरेलू चीज़ों के प्रति ‘राग-जिजीविषा में पवित्र भाव’ का स्मरण करते हुए उस मनोदशा से बाहर निकलने की सोचता है तो उसके आगे यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि “मैं भीतर से कितना बाहर हूँ.बाहर से सचमुच कितना भीतर मैं खुद आगे बढ़कर दर्पण में देखता हूँ. वहाँ जो दीख रहा है मेरा चेहरा नहीं.” इन पंक्तियों से गुज़रते हुए जहाँ एक ओर निराला की ‘बाहर मैं कर दिया गया हूँ भीतर पर भर दिया गया हूँ’ सरीखी काव्यपंक्ति का अनायास स्मरण हो आता है वहीं दूसरी और इक़बाल के एक शे’र की भी बेसाख्ता याद आती है:
तू बचा बचा के न रख इसे तिरा आइना है वो आइना
कि शिकस्ता हो तो अज़ीज़-तर है निगाह-ए-आइना-साज़ में.
कहा गया है कि सृजनशील मनुष्य जितना दुनियावी बाहरी झंझावातों से नहीं टूटता, उतना वह पारिवारिक क्लेश से टूटता है. अपने माता-पिता के जीवन संघर्ष से निर्मित जुझारू चेतना से लैस लेखक के कानों में पिता की वह कसमसाती आवाज़ आज भी गूँजती है जो उन्होंने पारिवारिक कलह से दुखी होकर अपनी पुत्रवधू द्वारा झोंपड़ी से निकाल दिए जाने और चू ल्हा-चौका अलग कर लेने पर कही थी : “ एक बार फिर वही कथा तीस साल पहले ऐसे ही बेघर हुए थे. मर-खप के जो घर बनाया, गृहस्थी जोड़ी, सब हाथ से गया.”(पृ.32) पुस्तक में विस्तार से ज़िक्र है कि कैसे घर से निकाले जाने के बाद एक लम्बे अरसे तक परिवार के बाकी सदस्यों ने मिलकर गोशाला की सफ़ाई की और जानवरों के साथ नए झोंपड़े में रहने को बाध्य हुए : “जानवर और आदमी एक छत के नीचे रह सकते थे.यह हमने उस समय जाना जबकि परिवार में मनुष्यों के साथ रहना दूभर था.” इतना ही नहीं, आगे ख़राब सेहत की वजह से पिता द्वारा खदान में मजदूरी का काम छोड़कर मजदूरों के लिए चाय-नाश्ते की दूकान शुरू करने पर बच्चों द्वारा स्कूली पढ़ाई से समय चुराकर भट्ठी सुलगाने से लेकर साफ़-सफ़ाई तक का काम अपने हाथ में लेते हुए माता-पिता की मदद करने का जैसा विस्तृत विवरण इस कृति में मिलता है वह लेखक के जीवन-संघर्ष के बहाने समाज के वंचित तबके के लोगों के जीवन की संघर्षगाथा है. उम्र के इस पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखने पर उसे ‘महुए की दरख़्त की छाँव में दो बच्चे अब भी कप-प्लेट धोते दिख पड़ते हैं.’
अमूमन संघर्षशील जीवन जीनेवालों के बारे में लोगों की धारणा होती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में सरसता का अभाव होता है. जबकि असलियत उलटी है. सुख-सुविधा सम्पन्न ज़िन्दगी नीरस और निरर्थक हो सकती है और जद्दोजहद से भरा जीवन भी सहज, स्वाभाविक और सरस हो सकता है. आलोच्य कृति में ऐसे अनेक प्रसंग वर्णित हैं जिनसे गुज़रते हुए हम खदान से लेकर खेती-पथारी करनेवाले लोगों को हँसते–गाते देख सकते हैं. उदाहरण के लिए मंडलोई जी ने कठोर श्रम करती पच्चीस वर्षीय लीला मजदूरिन के लोकगीत गाने का दिलचस्प चित्रण करते हुए लिखा है कि “जब वह गाती तो साथ में काम करने वाली ‘मेसो’ पीपे (टिन के कनस्तर) पर ताल देने लग जाती और सुर मिलाती. लीला में ग़जब की फुर्ती थी.वह चार बजे सुबह उठकर कुदाली उठा लेती और मिट्टी तोड़ना शुरू कर देती.बाक़ी मजदूरिनें उसके बाद पहुँचती.हम माँ के साथ जब पहुँचते तो वह मिट्टी तोड़ने का काम निपटाने के पास होती.हम देखते कि उसके गोर हाथों में कुदाली ऐसी लगती मानो तलवार लिए कोई देवी.” (पृ.37)
इसी प्रकार इंटरमीडिएट में पढ़ने के दौरान अपने एक शिक्षक के सौजन्य से पातालकोट में रहने वाले भारिया आदिवासियों के देखे सौन्दर्य का चित्रण करते हुए मंडलोई लिखते हैं : “छरहरे बदन. नाक चौड़ी किन्तु सुडौल.आँखें बनिस्बत छोटी.स्त्रियों के अधर पतले.दन्त पंक्तियाँ आकर्षक.श्यामवर्ण.गठा हुआ शरीर.देह चुस्त और गतिमय.भारिया पुरुष धोती,कुरता,बड़ी पगड़ी पहनते हैं. स्त्रियाँ लाल रंग की सेंदरी साड़ी और पोलका धारण करती हैं.गोदने से शरीर के अंगों का विन्यास करते हैं.भड़म,सैतम,और कर्म-सैला उनके प्रिय नृत्य हैं.ढोल,टिमरी, झाँझ, ढोलक, व बाँसुरी प्रमुख वाद्य.विशेष यह कि स्त्रियाँ मजीरा और चिटकुला बजाते हुए मदमस्त हो सब कुछ भूलकर नाचतीं-गातीं.” (पृ.195)
कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह बुर्जुआ सौन्दर्य के बजाए श्रम का सौन्दर्य है, जो श्रम करते वक़्त श्रम-परिहार के लिए गाते-गुनगुनाते-नाचते मेहनतकश स्त्री-पुरुषों को देखकर रचा गया और जिसका हिन्दी कविता में रूपायन करने के लिए अनेक प्रगतिशील रचनाकार और ख़ास तौर से केदारनाथ अग्रवाल सुप्रसिद्ध हैं.
मंडलोई महानगरीय दूरबीन से पिछड़े कहे जाने वाले इलाके के प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन-चित्रण करने वाले रचनाकारों से भिन्न उन लेखकों में से एक हैं जिन्होंने बचपन में प्रकृति को अपनी नंगी-खुली आँखों से एक लम्बे समय तक निहारा है. उनके यहाँ प्रकृति का मतलब केवल वन्य प्रकृति ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणी भी हैं: “गाँव के पास जो जंगल था, बचपन में उन्हीं के साथ घूमा.हमारी पहचान बरगद से हुई.कोई 200 फीट तक ऊँचा. बाढ़ महीने फूल.उसके फल गिलहरी को प्रिय.गिलहरी को इत्मीनान से फलों को कुतरते देखकर मैं हर्षित होता.उसकी कूद-फांद धरती से पेड़ तक.ग़जब की फुर्ती.लय और गति का अद्भुत मेल.कुल्लू का पेड़.इससे गोंद मिलती….मैंने जंगल में गूलर का पेड़ देखा….इसके फल लोमड़ी,चीतल,लंगूर और कई पक्षी खाते हैं.गिलहरी भी ख़ूब आनन्द के साथ जीमती है.”(पृ.41)
लेखक का कहना है कि प्रकट रूप में इन छोटे-छोटे वृतांतों ने उसके अंतर्मन को गहरे प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप उसके लेखन में गहन ऐन्द्रियता है. स्पष्ट ही यह तभी संभव है जब कोई रचनाकार अपने परिवेश से गहरे जुड़ा हो.इस कृति में जितने प्रकार के पक्षियों के नाम आए हैं उसे देखते हुए स्कौटिश-अमेरिकी कवि एवं पक्षी विज्ञानी अलेक्ज़ेन्डर विल्सन या ‘बर्डमैन ऑफ़ इण्डिया’ के नाम से मशहूर डॉ.सलीम अली की तर्ज़ पर मंडलोई जी को ‘आधुनिक हिन्दी साहित्य का बर्डमैन’ कहने को जी चाहता है. यह अलग बात है कि लेखक के पास पक्षियों के साथ साथ जंगली पशुओं, फलों और फूलों की भी अच्छी समझ है. ‘ऑनिˈथ़ॉलजि’ (पक्षी विज्ञान) से अनभिज्ञ किसी सुशिक्षित व्यक्ति को भी लेखक द्वारा सतपुड़ा के जंगल में पेंच नदी के किनारे उड़ते-तिरते दिखाई पड़े ‘पन कौव्वा’, ‘किलचिया’, ‘बड़ा बगुला’, ‘अंधा बगुला’, ‘सुरखाब’, ‘जलमुर्गी’ आदि के बारे में शायद ही पता हो. इसी प्रकार ‘चील’ और ‘बाज’ में फ़र्क अच्छे- अच्छों को मालूम नहीं होता. इनके अलावा विवेच्य कृति में राजहंस, सारस, तीतर, मोर, गौरैया, चिट्ठा, किलकिला, कोयल, तोता, नीलकंठ, कबूतर, मैना, कठफोड़वा, बुलबुल, चकदिल, और कोटवार आदि पक्षियों की चर्चा के मद्देनज़र यह कृति पक्षियों का विश्वकोश प्रतीत होती है. ऐसे परिवेश का चित्रण करते हुए आत्मकथा में कवित्व का प्रवेश लाज़िमी है. मंडलोई लिखते हैं : “मैं सोचता हूँ हम सरीखों का बचपन गरीबी में भी कितना अमीर था.हमारी आँखों में रंगों का विविध संसार था.कानों में कितनी मृदुल आवाजें.सुरों में विहँसता मन.स्पर्श में पक्षियों के कोमल अहसास.वनस्पतियों की अबूझ लेकिन मोहक सुगंधों का परिवेश.अनेक ध्वनियाँ जो सतपुड़ा में नदी,हवा,पेड़-पौधों,बादलों से झरतीं. वे मन को विरल उल्लास से भर देतीं.” (पृ.45)
सतपुड़ा के पशुओं में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, रीछ, सियार आदि के डर साथ ही चीतल, साँभर, नीलगाय,चौसिंगा,लोमड़ी, चिंकारा, खरगोश, बंदर, लंगूर के प्रति लेखक का आकर्षण उसकी रचनात्मकता को उद्बुद्ध करता रहा है. उसके शब्दों में इनसे “डर न लगता बल्कि दोस्ती करने का मन होता. ये सब ग्यारहवीं कक्षा तक जंगल के मिले सबक थे.इन्हें ही जीवन में पढ़ने का संकल्प लिए ,मैं अबतक भटक रहा हूँ.” इस क्रम में आत्मकथाकार द्वारा अपने अग्रज कवि जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध प्रगीत ‘बीती विभावरी जाग री’ के उल्लेख से कृति में जो वज़न पैदा हुआ है उसका अनुभव करने के लिए मूल पुस्तक पढ़ना अपरिहार्य है.
मंडलोई जी ने मीर तक़ी मीर को प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है: “वे अपने लिखे में पेड़-पौधों, दरख्तों, दरियाओं, समंदरों, आसमानों, पहाड़ों, पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं की बात करते,आज भी मौजू आदिवासी दर्शन के हमबगल दिखते हैं.जो कायनात को बचाने का अकेला उपाय नज़र आता है.”(रचना समय, अगस्त 1,2024)
तथाकथित विकास के नाम पर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाली योजनाओं को प्रश्नांकित करते हुए लेखक का कहना है कि “प्रकृति से अधिक उदार कोई नहीं.सभी के लिए उसके पास कुछ-न-कुछ ऐसा है, जो पूर्णत: नि:शुल्क है. जिनके पास पैसा नहीं, जो बेरोज़गार और ग़रीब हैं उनके लिए सदैव मौसम के अनुसार उपहार मौजूद है.” किन्तु, इससे यह निष्कर्ष निकालना ग़लत होगा कि मंडलोई जी का रुख प्रकृतिवादी और विकास विरोधी है.इसी पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि “ ऐसा नहीं कि प्रौद्योगिकी से बच्चों को कुछ न मिला हो. वह मिला है और मिलता रहेगा.दुनिया की तमाम खिड़कियाँ खुली हैं ज्ञान के साथ.उनके यथार्थ और सौन्दर्यबोध की भी खिड़की खुली रहे ताकि ऐन्द्रिय व्यवस्था जीवंत बनी रहे.”
विवेच्य रचना में अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए लेखक ने संभवत: अपनी ही तरह उपेक्षित दलित वर्ग से आने वाले ‘मास्साबों’ द्वारा परम्परा से प्रदत्त सामाजिक पदानुक्रम के दबाव में बच्चों के प्रति भेदभाव को उजागर करते हुए लिखा है कि कैसे मारपीट कर स्कूल की सफ़ाई का काम एक ख़ास तबके से आने वाले विद्यार्थियों से ही करवाया जाता था जिस कारण उन्हें स्कूल यातनागृह की तरह लगने लगता: “कुछ बच्चे तो जाति से साफ़-सफ़ाई की शानदार परम्परा वाले घरों से आए थे. जिनसे गोबर मल-मूत्र की सफ़ाई का काम लिया जाने लगा….जिन बच्चों ने साफ़-सफ़ाई के काम को हाथ में लिया जैसे वह उनका स्थायी काम हो गया.बस बाबू कॉलोनी के बच्चों को इस तरह के काम से मास्साबों ने डर के मारे मुक्त रखा.इस तरह ग़रीब-अमीर का विभाजन स्कूल में हो गया.” (पृ.47)
इस क्रम में विस्तार के साथ वर्णित है कि कैसे कुछ खदान मालिकों एवं अधिकारियों से दान में मिली टाटपट्टियों को बिछाने वाले निम्नवर्गीय परिवारों के विद्यार्थी उन पर बैठने से वंचित रह जाते थे. टाटपट्टियों पर बाबू कॉलोनी और समृद्ध परिवारों के बच्चों का अघोषित कब्ज़ा था.आदिवासी समाज से आनेवाले शिक्षक उनसे आत्मीयता से बातें करते और उनके सवालों के जवाब देते, पर मजूर परिवारों के बच्चों को झिड़क देते.इतना ही नहीं, उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती जिसमें पिटाई से लेकर स्कूल की सफ़ाई तक शामिल होती. नतीज़तन ऐसे बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति जन्म ले लेती जिस वजह से शिक़ायत घर पहुँचती और वहाँ भी ये बच्चे मार खाते. बावजूद इसके अगर लेखक ने पढ़ाई जारी रखी.: “हाथ में झाडू थी और पीठ पर उमचाती बेंत से निकलती चीखों में मजूर माँ-बाप का सपना था.”(पृ.50)
इस प्रसंग में सबसे भयावह घटना का ज़िक्र करना ज़रूरी है जब स्कूल के दिनों में परीक्षा में प्रथम आने के कारण लेखक से नाराज़ पांडे महाराज नामक सरपंच के भतीजे ने काफी दिनों तक गाली-गलौज और धमकी आदि के बाद फ़िल्म देखकर लौटते वक़्त उसे छुरा भोंक दिया:
“पाँजरा जंगल की चढ़ाई पैदल पार कर रहे थे.वह चढ़ाई जमकुंडा गाँव से लगी हुई थी. एक गाली उभरी – ‘… के, ले फर्स्ट आने का फल.’ मेरी बाईं पसली में छुरा घुस चुका था.वह पांडे महाराज का भतीजा था.छुरा निकालकर वह भाग चुका था….मैं अचेत-सा हो गया…पुलिस केस बन गया…घृणा की इस वारदात से घर में यह तय हो गया कि मैं अब इस गाँव में न रहूँगा.” (पृ.74)
मंडलोई जी की आत्मकथा में बारम्बार माँ और पिता का ज़िक्र मिलता है. इनमें कई ऐसे प्रसंग हैं जिनसे बाल्यावस्था में ही लेखक की सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता और परिपक्वता का पता चलता है.पिता नीम के पेड़ की महिमा बखानते न थकते. वे कहा करते थे कि ‘जो सुख पिता के कंधे पर सवार होने और माँ के आंचल में छुप जाने में मिलता है वही अनुभूति नीम की छाँह में है.’(पृ.190) माँ बालक लीलाधर के लिए एक अहसास थी.वह उसे उसके पसीने की गंध से पहचान लेता था.माँ के पास साड़ियाँ सीमित संख्या में थीं. जो थीं वे भी डीजल और घासलेट में खान की भूमिगत नौकरी में सनी थीं. बारबार धोने पर उनमें सूराख भले हो जाएँ पर उन पर लगे दाग़ छूटने का नाम न लेते.बावजूद इसके वह खान में काम करने जाते वक़्त अपने शरीर को अच्छी तरह ढँक कर ही जाती.लेखक के शब्दों में “घनघोर गर्मी के बावजूद लम्बी बाँहों का पोलका(ब्लाउज) जिसका गला ऊपर तक सिला होता था.एक मजदूरिन काम करते हुए उन तमाम जगहों पर पहले काम करती हैं जहाँ भूखी नज़रें कार्रवाई में सक्रिय होती हैं.”
माँ के साथ घर-घर चौका-बासन करने वाली रज्जो को लेखक ने ‘जीवन में पहली दोस्त’ और ‘सपनों की पहली प्रेमिका’ को लेखक ने ‘पहली कामगार लड़ाकू साथी’ के रूप में अभिहित किया है.रज्जो के दैहिक सौन्दर्य वर्णन का चित्रण करने के बावजूद भूख की वजह से पिसान के लिए बाबुओं का अनाज चक्की पर ले जाने के दौरान रास्ते में ही मुट्ठी भर-भर फक्का मारने लगने का जो चित्र खींचा गया है वह बेहद जीवंत है. पिसे हुए आटे की गंध से पागल-सी हुई रज्जो को आटा फाँकते देखकर वितृष्णा के बजाय उस पर प्रेम उमड़ आने के पीछे वह समवेदना है जो प्राय: एक तबके से आने वाले लोगों के साझा अनुभव की फलश्रुति हुआ करती है.
विवेच्य कृति में जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों और स्थितियों का विस्तार से वर्णन-चित्रण मिलता है उसके मद्देनज़र याद आ सकते हैं मिखाइल बख्तिन जिनका कहना है कि किसी कृति में अनेकस्वरता का समावेश उसे समृद्ध बनाता है. इस विश्लेषण-पद्धति के मूल में ‘पॉलीफोनी’ की अवधारणा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कई आवाज़ें. बख्तिन ने इसे संगीत से लिया है. इस पद्धति का अनुप्रयोग करते हुए दोस्तोयव्यस्की की रचनाओं को वे कई अलग-अलग आवाज़ों के रूप में पढ़ते हैं, जो एक ही परिप्रेक्ष्य में विलीन नहीं हैं और लेखक के निजी पूर्वग्रह के भी अधीन नहीं हैं. इनमें से प्रत्येक आवाज़ का अपना परिप्रेक्ष्य, अपनी वैधता और कृति के भीतर अपना कलात्मक वज़न है.
‘जब से आँख खुली हैं’ का लेखक भी अपनी आवाज़ को चरित्र और पाठक के बीच नहीं रखता, बल्कि उलट-पुलट करता है. ऐसा लगता है जैसे यह किताब कई पात्रों द्वारा लिखी गई हो. लेखक की आवाज़ द्वारा एक साथ रखी गई एकल वस्तुनिष्ठ दुनिया के बजाय इसमें चेतना की बहुलता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी दुनिया है.इस कृति का पाठक रचनाकार द्वारा प्रस्तुत बंधी-बंधाई वास्तविकता को नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि रचना में चित्रित प्रत्येक चरित्र को वास्तविकता कैसी दिखाई देती है.
आलोच्य कृति का पाठ अलग-अलग दृष्टिकोणों या विचारधाराओं की परस्पर अंत:क्रिया के रूप में प्रकट होता है, जो अलग-अलग चरित्रों द्वारा वहन किया जाता है. पात्र खुद के लिए बोलने में सक्षम हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे दूसरा व्यक्ति सीधे पाठ के माध्यम से बोल रहा हो.
कहना न होगा कि इकहरी संरचना वाली कृति में पात्र केवल लेखक की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए आते हैं और लेखक केवल अपने विचार का प्रतिनिधित्व करता है. पात्रों के बीच कोई भी अंतर एक ही चेतना के भीतर होता है. बख्तिन का कहना है कि ऐसी रचनाओं में कृति की पूरी संरचना एक ही स्वर से चिह्नित और सपाट होती है. वे ऐसे लेखकों की मंशा पर संदेह करते हैं , क्योंकि इसमें अक्सर दूसरे के नज़रिए की स्वायत्तता का सम्मान करने में लेखकीय विफलता को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता.
इसके विपरीत बड़े रचनाकार दृष्टिकोण की बहुलता को पहचानते हैं. इससे रचना में अनेकस्वरता पैदा होती है. ऐसे रचनाकार लगातार अन्य नज़रिए से जुड़ते हैं.उनसे प्रभावित होते हैं तथा उसमें से अपने लायक़ अंतर्वस्तु को ग्रहण करने और बेज़रूरी चीजों को छोड़कर कुछ सार्थक रचने का प्रयास करते हैं.तुलसीदास के शब्दों में कहें तो उनमें ‘संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने’ का विवेक हुआ करता है. रचना की यह प्रक्रिया प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या शैली से जुड़े पिछले इस्तेमाल पर आधारित होती है. बख्तिन के अनुसार भाषा-प्रयोग की यह शैली रोज़मर्रा की भाषा-प्रयोग की ख़ासियत है और साहित्यिक कृति में इसका प्रयोग भाषा-प्रयोग की वास्तविकता को सटीक रूप से दर्शाता है.
कहना यह है कि ‘जब से आँख खुली हैं’ के पाठ की संरचना इसमें चित्रित सारे पात्रों की प्रकृति के अधीन है. जाहिर है कि इस तरीके से रचित कृतियों को अनेक दृष्टिकोणों के बीच एक सम्प्रेषणीय संवाद के रूप में रचा जाता है. दूसरे शब्दों में इनमें विचारों को अमूर्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें जीवंत चरित्रों के माध्यम से मूर्त रूप दिया जाता है. विवेच्य कृति में अनेकस्वरता से भरपूर पाठ मानवीय संबंधों को यांत्रिक के बजाय संवादधर्मी रूप में प्रस्तुत करता है और यह लेखकीय यादृच्छिकता से बचा रह सका है. यह सही है कि क़लम रचनाकार के हाथ में होती है,पर जब तक वह यथार्थ की सहज-स्वाभाविक पुनर्रचना नहीं करता, उसकी कृति पठनीय और सार्थक नहीं हो सकती.
स्त्री-आत्मकथाओं के बारे में गरिमा श्रीवास्तव ने लिखा है कि जहाँ एक ओर ‘आत्मकथा के माध्यम से स्त्री-रचनाकार स्वयं को ‘खोजती’ है वहीं दूसरी ओर ‘स्त्रियों की आत्मकथाएँ उनके समुदायों की कथा के रूप में भी सामने आती हैं.’ (चुप्पियाँ और दरारें: ‘स्त्री-आत्मकथा:पाठ और सैद्धांतिकी’,पृ.22). प्रश्न है कि क्या पुरुष लेखकों की आत्मकथाएँ उनके समुदायों की कथा के रूप में सामने नहीं आतीं.स्पष्ट ही इस सवाल का ‘हाँ’ या ‘ना’ में दो टूक जवाब देना मुश्किल है.वजह यह कि जहाँ अभिजन पुरुष लेखकों की आत्मकथाओं में स्वभावत: निजता अधिक होती है,वहीं सबाल्टर्न समुदाय से संबद्ध ओमप्रकाश वाल्मीकि , माता प्रसाद, लक्ष्मण गायकवाड, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिशराय, श्यौराज सिंह बेचैन एवं लीलाधर मंडलोई सरीखे रचनाकारों की आत्मकथाओं में उनका अपना समुदाय और सामाजिक वर्ग किसी न किसी रूप में अवश्य रूपायित होता है. ‘मेरा प्रेम’ कविता में मंडलोई जी ने लिखा है:
मैं जो बोलता हूँ वह मेरा बोला नहीं
उसमें उनकी आवाज़ शामिल है
जो मेरी तरह बोलते हैं
उनके बोलने में प्रेम के अलावा
क्रोध, हिक़ारत और नफ़रत भी है
वे सिरे से बदसूरत करतूतों के ख़िलाफ़ हैं
मेरी आवाज़ में उनके क्रोध की समवेत चीख़ है
और नफ़रत में खौलते ज्वालामुखी की आग
वे इसमें उन्हीं चीज़ों को भस्म करना चाहते हैं
जो इस दुनिया के ख़िलाफ़ हैं
मैं उनके साथ हूँ इसलिए मेरी आवाज़ में उनका बोलना है
मैं अपने से अधिक उनके बोलने को प्रेम करता हूँ।
(‘जलावतन’, पृ.23)
आत्मकथाकार की अनुभूति की व्यापकता और गहराई और ख़ास तौर पर विभिन्न आदिवासी समुदायों की जीवनचर्या की प्रामाणिक जानकारी के मद्देनज़र यह कृति निस्संदेह ‘समाजविज्ञान का विज्ञान’ कही जा सकती है.वजह यह कि इसमें कुछ ऐसी अनुसूचित जनजातियों का विस्तृत एवं जीवंत चित्रण है, जिनका थोड़ा-बहुत ज़िक्र कुमार सुरेश सिंह ने ‘पीपुल्स ऑफ़ इंडिया’ शृंखला के तीसरे खंड के अंतर्गत लिखित ‘शेडुल्ड ट्राइब्स’ पुस्तक में किया है.
प्रोफ़ेसर योगेन्द्र सिंह साहित्यिक कृतियों और ख़ासकर उपन्यासों को ‘समाजविज्ञान का विज्ञान’(Science of Social Sciences) कहा करते थे.उनका मानना था कि श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के सर्जक रचना-क्रम में सामाजिक यथार्थ को प्राय: जिस गतिशील अवस्था में पकड़कर रूपायित करने में समर्थ होते हैं वह तमाम तरह के आंकड़ों के वर्गीकरण के बाद विश्लेषण करने पर भी समाजविज्ञान में संभव नहीं हो पाता.
अंतिम बात यह कि मनुष्य देवताओं से इसलिए भिन्न है, क्योंकि वह दूध का धुला नहीं होता.उसमें प्राय: कोई न कोई मानवीय दुर्बलता होती ही है. ग़ालिब इस सच को बयान करते हुए कहते हैं:
मैंने लड़कपन में मजनूँ पे ‘असद’
संग उठाया था कि सर याद आया
गौरतलब है कि विश्व साहित्य में वे ही आत्मकथाएँ कालजयी मानी गयी हैं जिनके लेखकों ने कई प्रसंगों में खुद को कटघरे में खड़ा करके अपने व्यक्तित्व, चरित्र, जीवन में लिए गए किसी ग़लत निर्णय एवं आचार-व्यवहार से जुड़ी दुर्बलताओं को खोलकर सामने रख देने का साहस किया है.इस दृष्टि से संत अगेस्टीन और रूसो के ‘कंफेशंस’, ‘ख़ुद को अपनी पुस्तकों का विषय’ बतानेवाले मांतेन की आत्मकथा( Essais), ‘शानदार लेखक और एक भयानक व्यक्ति’ (Brilliant writer and terrible person) के तौर पर ख्यात हेमिंग्वे रचित ‘अ मूवेबल फीस्ट’ के साथ ही गांधी की ‘सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा’ सरीखी पुस्तकों का महत्त्व स्वयंसिद्ध है. आलोच्य आत्मकथात्मक कृति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें लेखक ने अपनी किसी भी दुर्बलता को प्रकट होने से सावधानीपूर्वक बचा लिया है. इसे हम एक रचनाकार के रणनीतिक कौशल के रूप में भी देख सकते हैं. संभव है कि आत्मकथा के दूसरे भाग में यह आलोचकीय शिकायत दूर हो जाए.
बावजूद इसके कहना न होगा कि आत्मकथा की वैधानिक एवं भाषिक संरचना के मद्देनज़र हिन्दी में आत्मकथा लेखन की समृद्ध परम्परा में लीलाधर मंडलोई की ‘जब से आँख खुली हैं’ एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कृति है.
(लीलाधर मंडलोई : ‘जब से आँख खुली हैं’, राजकमल पेपरबैक्स, मूल्य : ₹350, कुल पृ.246)
प्रोफ़ेसर रवि रंजन
जन्म : मुजफ्फरपुर.
शिक्षा : पी-एच.डी.
रूचि के क्षेत्र : भक्तिकाव्य, आधुनिक हिन्दी कविता, आलोचना, साहित्य का समाजशास्त्र.
प्रकाशित कृतियाँ : ‘नवगीत का विकास और राजेंद्र प्रसाद सिंह’, ‘प्रगतिवादी कविता में वस्तु और रूप’,.’सृजन और समीक्षा:विविध आयाम’, ‘भक्तिकाव्य का समाजशास्त्र पदमावत’, ‘अनमिल आखर’ , ‘आलोचना का आत्मसंघर्ष’ (सं) वाणी प्रकाशन,दिल्ली (2011), ‘साहित्य का समाजशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र: व्यावहारिक परिदृश्य’ (2012), ‘वारसा डायरी’(2022), ‘लोकप्रिय हिन्दी कविता का समाजशास्त्र’
प्रतिनियुक्ति : 2005 से 2008 तक सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़, पेकिंग विश्वविद्यालय,बीजिंग एवं नवम्बर 2015 से सितम्बर 2018 तक वारसा विश्वविद्यालय,पोलैंड में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा विज़िटिंग प्रोफ़ेसर के रूप में प्रतिनियुक्त.
सम्प्रति: प्रोफ़ेसर एवं पूर्व-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मानविकी संकाय, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500 046
ई.मेल. : raviranjan@uohyd.ac.in मो.9000606742
Discover more from रचना समय
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

