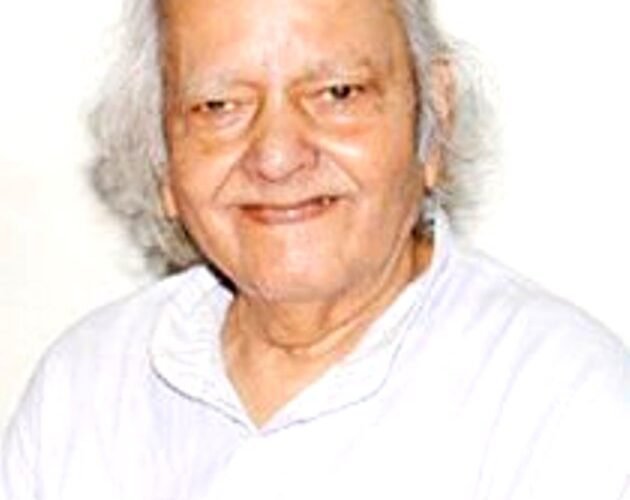पुनर्पाठ
1925 ई. में जनमें अमरकान्त हिन्दी के एक श्रेष्ठ कथाकार रहे। है उनकी ’डिप्टी कलक्टरी’ कहानी 1955 में प्रकाशित हुई थी। तब नयी कहानी आन्दोलन के पचासोत्तर युग में इसी कहानी ने उनकी पहचान बनायी थी। यद्यपि इसके पहले से वह कहानियाँ लिख रहे थे। पर उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाया था। जब पहली बार उनकी ओर ध्यान गया तब यह लगा कि अमरकान्त के नाम के बिना नयी कहानी की चर्चा अधूरी है। मुझे उनकी चार (4) कहानियाँ ’मील के पत्थर’ जैसी लगती हैं- 1. डिप्टी कलक्टरी, 2. दोपहर का भोजन, 3. ज़िन्दगी और जोंक और 4. हत्यारे। उनके 17 कहानीसंग्रह और 11 उपन्यासकृतियाँ प्रकाशित हैं। मेरा मानना है कि अमरकान्त की कहानियों पर गहराई से विचार करने वाला, उनमें छिपी दूसरी संरचना को उद्घाटित करने वाला कोई आलोचक अब तक हिन्दी में नहीं आ पाया है।
अमरकान्त की कहानी के आलोचकों में प्रायः छह आलोचकों के नाम लिये जा सकते है- 1. नामवर सिंह, 2. राजेन्द्र यादव, 3. विश्वनाथ त्रिपाठी, 4. सुरेन्द्र चौधरी, 5. रविभूषण और 6. मार्तण्ड। उनकी एक विशेष कहानी ’हत्यारे’ पर इन सभी आलोचकों ने समयसमय पर विचार किया है। पर कोई भी कहानी के अन्तर्कथ्य को नहीं खोल सका है। कहानी के पाठ से जुड़ने की और उसके साभिप्राय अर्थगह्वर में प्रवेश करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की है। बिना उससे जुड़े और उसे आत्मसात् किये ’हत्यारे’ के अर्थगह्वर को खोलना मुमकिन भी नहीं है। कहना न होगा कि ये तथाकथित पारखी आलोचक मार्क्सवादी हैं। अतः पाठ ;ज्मगजद्ध से सामान्यतः ये नहीं जुड़ सकते थे। इनमें से जिन तीन आलोचकों का देहान्त हो चुका है वे है 1. सुरेन्द्र चौधरी, 2. नामवर सिंह और 3. राजेन्द्र यादव।
प्रश्न उठता है कि क्या कहानी मार्क्सवाद, अस्तिववाद या समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के चश्मे से ही देखी और समझी जा सकती है और अगर देखी जा सकती है, तो देखना यह होगा कि आप इन सब माध्यमों से कहानी की कैसी और कितनी अन्तर्हित साभिप्रायता को उद्घाटित कर पाये हैं।
संदर्भतः बता दूँ कि हरिशंकर परसाई को यह गुमान और मुगालता था कि साहित्यकार केवल सर्जक हो सकता है, आलोचक कभी नहीं हो सकता। यह बात उन्होंने धनंजय वर्मा को लिखी थी। इधर सुरेन्द्र चौधरी और नामवर सिंह यह मानकर चलते हैं कि सर्जक साहित्यकार के लेखन को संशोधित करने का अधिकार आलोचकों को प्राप्त है। इसी अधिकार से सुरेन्द्र चौधरी ’हत्यारे’ के विषय में कहते हैं कि इस कहानी में हत्या नहीं की जानी चाहिए थी। पर नामवर सिंह इससे सहमत नहीं होते और अमरकान्त के पक्ष में खड़े होकर कहते है कि हत्या के बिना यह कहानी कहानी ही नहीं बन पाती। यानी हत्या इस कहानी के कथ्य के लिए जरूरी है। पर ये दोनों इस कहानी में कथ्य की अन्तर्निहित सार्थकता और साभिप्रायता पर विचार नहीं कर पाते है। राजेन्द्र यादव इसमें संघर्ष नहीं देखते, जो इसमें है भी नहीं। पर कहानीकार के आत्मसंघर्ष की ओर उनका ध्यान नहीं जा पाता, जिसके कारण ही यह कहानी रची जा सकी है। राजेन्द्र यादव न केवल इस कहानी को, बल्कि इसके कथाकार अमरकान्त को ही अस्तित्ववादी कहानीकार घोषित कर देते है। विश्वनाथ त्रिपाठी की दृष्टि भी इस बात पर जाकर टिक जाती है कि इस कहानी में संघर्ष का अभाव है और वह इस कहानी के दोनों युवा पात्रों को जयप्रकाश के आन्दोलन के बाद उससे निकले युवकों के रूप में देख लेते है। ध्यान दीजिए ’हत्यारे’ कहानी 1962 में लिखी जाती है और जयप्रकाश का आन्दोलन 1974 में शुरू होता है। ऐसे में उक्त कथन कितना उचित हो सकता है? यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह कहानी अपने स्वरूप में जिस तरह है, कहानी का पाठ Text जिस रूप में रचा गया है, उसके उस स्वरूप के साथ ही उसपर विचार होना चाहिए, जो ये आलोचक नहीं कर पाते हैं।
पाँचवें आलोचक रविभूषण जी है और छठे आलोचक मार्तण्ड जी। मैंने आधा दर्जन इन मार्क्सवादी आलोचकों की ’हत्यारे’ कहानी से जुड़ी आलोचना पढ़ी और सुनी है। पाँचवे और छठे आलोचकों का आलोचनापाठ दोतीन बार इस आशा से सुना है कि उसमें कहीं कुछ कहानी के विषय में महत्त्वपूर्ण मिल पाये, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी है। इस कहानी में किसी भी आलोचक के द्वारा परकायप्रवेश संभव नहीं हो सका है और न इस कहानी को कोई आत्मसात् ही कर सका हैं। यह तो तभी संभव है जब इसके कथ्यगह्वर में इनको एंट्री मिल पाती है। हाँ, परवर्ती दो आलोचक ’हत्यारे’ को बेस बना कर भानुमती का कुनबा अवश्य जोड़ते और दूर की कौड़ी लाने में जरूर माहिर सिद्ध होते है। कहानी के समकाल की जगह उससे बाहर आकर ये ’आज के समय’ को खोजने लगते हैं। रविभूषण 1944 से ’आज का समय’ को रेखांकित और परिभाषित करने लगते हैं। पर उनसे असहमत मार्तण्ड इसे इसके बाद के समय में रेखाकित करने लगते है। यहां एक सहज पाठकीय प्रश्न उठता है कि इस समय को कहानी में क्यों नहीं खोजा जाता और अपने समकाल और भविष्य से ही इसे क्यों नहीं जोड़ा जाता? ’हत्यारे’ कहानी में आज का समय मूर्तिमान है। इस समय को पहचाननेपहचनवाने और रेखांकित करने का काम आलोचक का है। पर रविभूषण और मार्तण्ड-दोनों ही काल को बाहर से लाकर ’हत्यारे’ पर आरोपित करते है और उसके आधार पर कहानी की पहचान करना चाहते है। रविभूषण वैश्विक काल को उठा लाते हैं। मार्तण्ड भी कहानी में निरूपित काल को या समय की जिस कोख ने इस रचना को जन्म दिया है,उसे निरूपित नहीं कर पाते हैं। वह अपने ज्ञान का विभ्राट् आडम्बर रचते हैं। ऐसा ही आडम्बर अपने ज्ञान का मार्तण्ड भी रचते हैं। रविभूषण इस कहानी को समझने के लिए विभिन्न पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के और उनकी पुस्तकों के नाम तक गिना देते हैं और आर्थिक नीतियों की चर्चा भी करते हैं। कहानी में केवल एक प्रधानमंत्री-प्रथम और तद्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल की साभिप्राय चर्चा है। पर रविभूषण अपने देश के कई प्रधानमंत्रियों के नाम गिना जाते हैं- उसे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तक खींच ले आते है। मार्तण्ड ’डिमिस्टिफिकेशन’ जैसे पद की बात करते हैं। बकौल मुक्तिबोध साहित्यकृति अपनेआप में एक फैंटेसी होती है। ’हत्यारे’ भी एक ’फैंटेसी’ है। इसका यथार्थ भी ’फैटेंसी’ में व्यक्तअव्यक्त है। पर मार्तण्ड इसे ’डिमिस्टिफाह’ नहीं कर पाते। रविभूषण कहानी में दायेंबायें को पकड़ते हैं और उन्हें अंधा युग के दोनों प्रहरी याद आ जाते हैं। मार्तण्ड कहानी की आखिरी पंक्ति के ’अंधरे’ को पकड़ते हैं और उन्हें मुक्तिबोध की ’आंँधेरे में’ कविता याद आ जाती है। उन्हें सार्त्र की कहानी Killer की भी याद आती है। पर उसके कथापाठ को उदाहृत करके भी वह उसे इस कहानी का सार्थक अन्तरपाठ Inter-Text नहीं बना पाते है। सूर्य के ये दोनों पर्याय (रविभूषण और मार्तण्ड) ही जब इस कहानी के अंधेरे को छांट कर उसके कथ्य को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, तब इनके सामने नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी और राजेन्द्र यादव की भला क्या बिसात रह जाती हैं और सुरेन्द्र चौधरी का ’स्वीपिंग रिमार्क’ कि कहानी में हत्या नहीं की जानी चाहिए थी- कहानी के बीज कथ्य से ही उनके अपरिचय को सामने ले आता है। वह इस कहानी की रचनाप्रक्रिया को ही नहीं समझ पाते हैं। ऐसी गलत बयानी उनकी कहानी की समझ पर ही बड़ा प्रश्नचिह्न बन जाती है। राजेन्द्र यादव के लिए ’हत्यारे’ अस्तित्ववादी कहानी है और अमरकान्त अस्तित्ववादी कहानीकार है। राजेन्द्र यादव की यह उतनीही बड़ी नासमझी है, जितनी बड़ी नासमझी कभी रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अँधेरे में’ कविता को अस्तित्ववादी कविता कहकर प्रकट की थी। ’हत्यारे’ में अपराध तो है, पर अपराध का राजनीतीकरण और राजनीति का अपराधीकरण नहीं है। चालू और पोपुलर शब्दों के प्रयोग का मोह किसी कहानी की समझ की कितनी बेरहम हत्या कर देता है इसका यह बहुत बड़ा दृष्टांत है। मार्तण्ड को फासीवाद ’पेटीबुर्जुआ’ और लुम्पेन-सभी पद याद आ जाते है। पर इस कहानी में इन पदों को समझने से कहाँ क्या मदद मिलती है- इसे वह कहीं भी नहीं बता पाये हैं। श्रोता के सामने तो उनका सारा वादज्ञान तो उभरता है, पर कहानी दब जाती है। वस्तुतः यह कहानी से दूर निजी ज्ञान का पाखंड और जनवाद का प्रपंच रचते है, कहानी की आलोचना नहीं करते है।
अपनी प्रतिबद्ध विचारधारा वाले इन आलोचकों में से किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा सका कि इस कहानी में ’हत्यारे’ कौन है? रविभूषण और मार्तण्ड कहानी में आये एक किताब के नाम को पकड़ लेते हैं- The grammar of Politics (Harold Laski) पर Grammar of Language पर उनका ध्यान नहीं जा पाता। कहानी में हत्या एक युवक-गोरा-करता है। दोनों हत्या नहीं करते। फिर इस कहानी का शीर्षक एक वचन में ’हत्यारा’ क्यों नहीं है और बहुवचन में अमरकान्त के द्वारा ’हत्यारे’ लिखने का क्या औचित्य है? क्या यह कहानी के पाठक को कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं करता?
’हत्यारे’ कहानी के लिखे जाने का समय 1962 है, जिसे अन्तिम दो आलोचकों ने उसे नेहरू का अवसानकाल माना है। मार्तण्ड उसे मोहभंग का काल मानते हैं। नेहरू का यह अवसानकाल तो अवश्य है, पर ऐसा कहने की जगह उससे बेहतर यह कहना होगा कि यह उनकी विफलता का काल है। इसके कई कारण हैं। अतः यह मोहभंग का काल नहीं है। मोहभंग 1967 के चुनाव के परिणामों से उजागर होने लगता है। हाँ, 1962 में पहली बार राममनोहर लोहिया संसद में चुनकर आते हैं और वह संसद में अंग्रेज़ी में बोलते हुए जवाहर लाल और कांग्रेस को ’दोजीभे’ कहकर सम्बोधित करते है।
सर्वपल्लि राधाकृष्णन (पूर्व राष्ट्रपति) के सुपुत्र गोपाल राधाकृष्णन ने यह लिखा है कि नेहरू अपने अंतिम दिनों में यह महसूस करने लगे थे कि एक अवांछित भारत WRONG INDIA उभरने लगा है। इसका उन्हें खेद और दुःख भी था। ’हत्यारे’ कहानी नेहरू के द्वारा महसूस किये गये इसी कालखंड में उभरने वाले अवांछित भारत WRONG INDIA पर लिखी गयी कहानी है। यह तब का सन्दर्भ है, जिसमें यह कहानी अपनी सार्थकता प्राप्त करती है और भविष्य तक को आत्मसात कर लेती है। नेहरू ने जिस ’रांग इंडिया’ को उभरते हुए देखा था, अमरकान्त ने ’हत्यारे’ कहानी में इसी को साकार कर दिया है। पर यह बड़े कलात्मक रूप में हुआ है। कहानी के पाठक के लिए इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है, न कि यथार्थवाद को और न ही यथार्थवाद के अन्दरूनी धड़ों को यहाँ समझने की अपेक्षा है। इस प्रकार यह नेहरू के ’रांग इंडिया’ वाले समय से अब तक उसी दिशा में लगातार बढ़ते चले आ रहे समय की अन्तर्कथा है। इस छोटीसी अन्तर्भेदी दृष्टि और नेहरू की विफलता के पर्यवेक्षण के अभाव में ’आज का समय’ को बाज़ारवाद पर आयी 1944 में छपी किताब में ढूँढना निरा हास्यस्पद लगता है। वस्तुतः ’रांग इंडिया’ का उभरना अपने देश में एक पूरेकेपूरे वर्ग का उभरना है, जो तब निरुपाय नेहरू की चिन्ता का विषय बना था। पर ’इस रांग इंडिया’ को उभरने देने वाले शासक नेहरू ही तो थे और उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले भी स्वयं नेहरू ही थे। इसे नियंत्रित करना, रोक पाना जब नेहरू के वश का नहीं रहा, तभी उन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति की थी। अमरकान्त नेहरू को मानते थे। वह उन्हें सच्चा गाँधीवादी भी समझते थे। यह उनकी निजी समझ थी। रवीन्द्र कालिया के अनुसार अमरकान्त को गाँधी और नेहरू पसन्द थे। उनके शब्दों में अमरकान्त नेहरूवादी थे। पर अमरकान्त का यह भ्रम 1962 तक आते-आते ठीक वैसे ही टूटा, जैसे परवर्ती नेहरू काल में 1962 में दिनकर का भ्रम ’परशुराम की प्रतीक्षा’ लिखते समय अपने लोकनायक से टूटा था।
अमरकान्त की कहानी ’हत्यारे’ के दोनो पात्र इस ’रांग इंडिया’ की कोख से पैदा हुए हैं। ये उस वर्ग का ही प्रतिनिधत्व करते हैं। इनमें कर्मसंस्कृति का कहीं लेश भी नहीं है। ये कामचोर और बातें बघाड़ने वाले सुखभोगवादी हैं। इन्हें समाज, राजनीति, शिक्षा- सबका पल्लवग्राही ज्ञान है। व्यापकता तो उनमें है, पर उसकी केन्द्रीयता और गहनता का उनमें घोर अभाव है। पर उनकी आपसी बातचीत एबसर्ड नहीं है। वह एक फैंटेंसी तो है, पर इसमें समाज, राजनीति और शिक्षा से संदर्भित वह पूरा समकाल उजागर हो जाता है। इनमें स्वेच्छाचारिता है, लूटमार करने और हत्या करने, देहभोग तक कर आने की उच्छंखल कर्महीन सुखोपभोगी प्रवृति है। इसीलिए ये’ रांग इंडिया’ वाले वर्ग के प्रतिनिधि हैं।
आजकल साहित्य के पीठाधीश जनवादी आलोचक अमरकान्त की ’हत्यारे’ कहानी पर विचार करने के क्रम में उसकी ’डिप्टी कलक्टरी’, ’दोपहर का भोजन’, और ’जिन्दगी और जांेक’। जैसी कहानियों का नाम लेते ही ऐसा नाकभौं सिकोड़ते हैं, मानों पाठक और साहित्यचिन्तक अमरकान्त की कैसी पिछड़ी बीती कहानियों का उल्लेख कर रहे हैं और कहानी के ऐसे पाठकों को बहुत पिछड़ा हुआ कथापाठक मानने लग जाते हैं। मुझे ऐसे पीठाधीशों के साहित्यविवेक पर तरस आता है। जनवादी आलोचक साहित्य को प्रायः युग या कालसापेक्ष मानते है, फिर भी इन तीनों कहानियों और ’हत्यारे’ के लेखनकाल को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं कि किसी साहित्यकार या कहानीकार की एक रचना अथवा एक कहानी के आधार पर उसका मूल्यांकन कर देना कभी समीचीन नहीं है। बकौल मुक्तिबोध किसी भी साहित्यकार (या कहानीकार) का मूल्यांकन उसके समग्र साहित्य को पढ़ने के बाद ही किया जाना चाहिए, किन्हीं एकदो कृतियों के आधार पर नहीं, अन्यथा वह मूल्यांकन सदैव अधूरा ही माना जाएगा।
’हत्यारे’ कहानी सातवें दशक के आरंभ में (1962) में लिखी गयी थी। तब नामवर सिंह ’नयी कहानी’ आन्दोलन में ’एक और शुरूआत’ की बात कर रहे थे। उन्हें ज्ञानरंजन काशीनाथ सिंह और दूधनाथ सिंह ही दीख रहे थे। पर उन्हें एक और शुरूआत का सबसे अधिक सटीक साक्ष्य देने वाली यह कहानी (हत्यारे) और उसके लेखक अमरकान्त की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही थी। ’डिप्टी कलक्टरी’ और ’दोपहर का भोजन’ मध्यवर्गीय परिवार की कहानियाँ हैं और ’ज़िन्दगी और जांेक’ लोकमानस के बीच जिजीविषाबोध की कहानी हैं। एक जनवादी आलोचक ने इस ’हत्यारे’ कहानी को अमरकान्त की कहानियों में एक ’ब्रेक’ माना है। पर यह कहानी अमरकान्त की कहानियों में एक ब्रेक नहीं होकर एक ’शिफ़्टसी’ लगती है। मूलतः यह ’शिफ़्ट’ भी नहीं रह जाती, बल्कि ’ग्रोथ’ बन जाती है। कहना होगा कि यही कहानीकार के रूप में अमरकान्त की सफलता है।
रविभूषण जी ने जनवादी कथामंच से इस कहानी का विवेचन और मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। यह अच्छी बात है कि वह इस कहानी का अपना विवेचन कहानी के पाठ Text के आधार पर करते हुए चलते हैं। पर वास्तविक स्थिति पाठ Text की ऊपरी सतह से गुजर जाने की ही है। अतः कहानी का ’पारफ्रेज’ करते हुए वह जगहजगह पर जनवादी धारणाओं का दस्तावेजीकरण इस कहानी पर चस्पा करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि कहानी का पाठ इनसे छूट जाता है और उनकी विश्वदृष्टि उनपर हावी हो जाती है। पर मेरे लिए यह कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मुक्तिबोध से भी होता रहा है और मैनेजर पांडेय से भी। फर्क इतना ही है कि मुक्तिबोध और मैनेजर पांडेय को यह मुगालता नहीं होता है या उनका विवेचन ऐसा नहीं लगता है कि उनके द्वारा गृहीत रचनाविशेष को सिर्फ उन्होंने ही समझा है, औरो ने नहीं या कि उनके सिवा और सब नासमझ है- पर रविभूषण जी को यह प्रतीति अवश्य होती है।
’हत्यारे’ पर मैं अपनी बात कुछसवालों से आरम्भ करना चाहता हूँ। आखिर इस कहानी में हत्यारे कौन हैं और हत्या किसकी होती है? जितना कहानी में सरसरी तौर पर पाठ में नजर आता है, इसका उत्तर उतना भर ही है, या यहाँ कुछ अन्तर्निहित भी है? अगर है, तो आलोचक उसकी बात क्यों नहीं करना चाहता है? रविभूषण जी की कठिनाई यह है कि वह पाठ को समग्रता में, उसके पूरेपन में देखनासमझना नहीं चाहते। जहाँ कहीं उन्हें कुछ संकेतसंकेतित नज़र आता है वह उन्हीं स्थलों की बात करते हैं- ’हत्यारे’ कहानी को छिटपुट सतही संकेतों से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं यानी पूरा कथापाठ Text संसक्त रूप में उनकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह उनसे छूट जाता है। वह बायें और दायें की सांकेतिकता को पकड़ते है, वह ’इंडिविजुअल’ को ’इंडिविजुअल’ नहीं रहने देना चाहते है पर उसकी गहरी अर्थवत्ता को उसकी व्यक्तिपरकता में गोताखोरी कर नहीं तलाशना चाहते है। उसे वह तत्काल ’वर्ग’ से जोड़ देते हैं। पर वह जिस वर्ग को कहानी में ढूँढ लेते हैं वह इस कथापाठ में उस रूप में है ही नहीं जिस रूप में वह रविभूषण जी को काम्य है। रविभूषण जी यह नहीं देख पाते कि बायें और दायें को उनके द्वारा घूर कर देखा जाना’- यहाँ दोनों की उपेक्षा है, दोनों के विफल रह जाने की, उनके सार्थक सिद्ध नहीं हो पाने की स्थितिदृष्टि है। वह ’दायें’ और ’बायें’- दक्षिण और वाम- दोनों ही अनैतिक है, दोनों ही बेईमान है, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। अतः दोनों ही से इन्हें घृणा है, नफरत है। वह न सत्तारूढ़ दल की ओर जाता है और न प्रतिपक्ष की ओर, न दक्षिणपंथियों की ओर जाता है और न वामपंथियों की ओर। वह तो अँधेरे में गुम हो जाता है। वह Wrong India को सिरजने वाला एक तीसरा वर्ग बन जाता है, जिसके तथ्य को जानकर नेहरू चिंतित हो उठे थे। यह एक प्रकार का प्रतिसमाज है, Anti Society है। यही Wrong India को ’अवांछित भारत’ को निर्मित करने वाला वर्ग है। कहानी का यह अंतिम अंधेरा वस्तुतः प्रतिसमाज Anti-Society का अँधेरा है। ये दोनों अपने इसी आश्रय और गम्य स्थान की ओर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ ये सुरक्षित हैं।
कहानी में गरीब तबके की, चूल्हे पर खाना बनाने वाली वह औरत जो अपने आर्थिक अभाव में अपने मर्द के रहते हुए भी अपनी देह बेचती है, वह इंडिविजुल’ नहीं है, तो वह समाज में उत्पन्न इस तरह के वर्ग को ही प्रतीकित करती है, उस व्यापक दलितदमित शोषित वर्ग को संकेतित नहीं करती, जिसकी ओर रविभूषण जी का संकेत है। रविभूषण जी की मुश्किल यह है कि जबतक कहानी के पाठ Text को अपनेआप मे पूरी तरह खोल नहीं दिया जाए या समझ और समझा नहीं दिया जाए, तब तक अन्तरपाठ Inter Text का उल्लेख कर देना भी उचित नहीं है। उसका पति अपने बाप के साथ वहीं बाहर बेफिक्र बैठा, भात खा रहा होता है। वह अगर इंडिविजुअल नहीं है तो आलोचक के अभीष्ट क्लास को भी प्रतिबिंबित नहीं करती, अपितु कहानी के साँचे में वह अपनी गुणात्मकता में कर्मसंस्कृति को प्रतीकित करती है। अब ऐसे में तन बेचने वाली इंडिविजुअल और कर्मसंस्कति को संकेतित करने वाली वुधिया- दोनों समाज कैसे हो सकते हैं? इसी तरह बोध के अँधेरे में इस अंधेरे से वैसे और कितनी दूर तक सही साम्य बिठाया जा सकता है- इस ओर भी रविभूषण जी का ध्यान नहीं जा पाता। असल में इस कहानी में जो ’हत्यारा’ दीखता है, वह वास्तव में हत्यारा है नहीं, हत्यारे तो वे हैं जिनका कहानी में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है- पर इस ओर कहानी के पाठक का ध्यान नहीं जा पाता है। कहानी में जो प्रत्यक्ष ’हत्यारा’ है उसके पहले इस कहानी में कितने हत्यारे है इसे तलाशने अन्वेषित करने की अपेक्षा है। कहानी में जो प्रकट तौर पर हत्या दिखाई जाती है- उसका कारण क्या है? यहाँ हत्या का पहला कारण है गरीब स्त्री से अपनी यौनेव्छापूर्ति कर उसे रुपये न देकर चार रुपये बचा लेने की प्रबल इच्छा, यानी लूट लेने की संकल्पि इच्छा। यहाँ जो उसे पकड़ने वाला आ रहा आदमी जब उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी उससे अपने रुपये बचाने और पकड़ जाने से बचने के लिए रोशनी में आते ही वह उसकी हत्या कर देता है। यहाँ ’हत्यारे’ कहानी की तुलना रघुवीर सहाय की कविता ’रामदास आज मर गया’ से भी कर दी जाती है। पर उस कविता में मारे जाने के कारण का पता नहीं चलता। वहाँ कारण नहीं दिया गया है । पर इस कहानी में मारे जाने का कारण सुस्पष्ट हैं। इसमें वह कहानी में प्रकट है। पर जो हत्या होती है वह लूट कर और एक तरह से रेप कर भागने वाले की पकड़ से बचने के लिए होती है। पर ऐसी अनेक हत्याएँ यहाँ अतर्गर्भित हैं। इन्हें देखे जाने और दिखाने की जरूरत है। रामदास के मरने के अन्तरपाठ के उल्लेख से अन्तर्गर्भित हत्याएँ नहीं उकेरी जा सकती हैं।
कहानी में दोनों पात्रों के रंग का भी उल्लेख है- एक गोरा है, तो दूसरा गहरे सॉवले रंग का है। यहाँ दक्षिणपंथी और वामपंथी- दोनों ही ’रांग इंडिया’ को सिरजने, उत्पन्न करने वाले हैं। ये कहानी में अपनीअपनी भागीदारी निभाते हैं। कहानी में मज़े का ऐसा हर प्रसंग इन दोनों ही- दक्षिणपंथी और वामपंथी- से जुड़ा हुआ है।
’हत्यारे’ कहानी में शिक्षा का परिवेश अग्र प्रस्तुत है। यह कहानी के बीजसूत्र को विकसित होने के बाद आता है। इस शैक्षणिक परिवेश में प्रोफ़ेसर है और शोधार्थी, विद्यार्थी भी हैं। कहानी के दोनों पात्र भी एम.ए. उत्तरार्ध के विद्यार्थी प्रतीत होते है। इनके तद्कालीन शैक्षणिक परिवेश का यह एक उदहारणमात्र है। पर यहाँ दोनों की तद्कालीनता में, राजनीति, में समाज में अभियांत्रिकी के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, नेताओं और मंत्रालयों की रूटीनी कर्मचर्या में- सबकहीं ऐसी ही स्थिति है। कहानी न होकर यदि यह उपन्यास के रूप में लिखा जाता, तो इन सारे क्षेत्रों से भी ऐसी सारी स्थितियाँ उजागर कर दिखा दी जातीं। पर यहाँ एक क्षेत्र के घोर पतन को उद्घाटित कर अन्य क्षेत्रों की ओर सहज ही संकेत कर दिया गया है, जिसका भान पूरी कहानी पढ़ लेने के साथ हो जाता है।
रविभूषण जी इस कहानी का विवेचन करते हुए एकाधिक बार यह बताते है कि इस कहानी का हर वाक्य कसा हुआ है। मुझे थोड़ा विस्मय होता है कि भाषा को महत्त्वहीन मानने वाले जनवादियों को भूलकर यहाँ आलोचक का ध्यान बाक्य की ओर आखिर क्यों गया है? दरअसल जिसे वह बताना चाहते हैं, वह बाक्य नहीं है बल्कि पूरी कहानी का डिस्कोर्स है। कहानी का कथनविधान है। वहां बाक्यों की आपसी संसक्ति से यह कथन बनता है, उक्ति या प्रोक्ति बनती है। कहानी केवल अपेक्षित को कह कर ही बुनी गयी है, जहाँ कथन, परस्पर पूरी तरह कंडेंस्ड हैं सुसंहत हैं। कहानी में ऊपर से जो विसंगत या एब्सर्ड है, उसके भीतर इनकायथार्थ भरा पड़ा है। वह कहानीकार का विशिष्ट कौशल है। उसने ’फेला’ को ’सुजेत’ में बदल दिया है। यथार्थसंख्या एक को यथार्थसंख्या दो में रूपांतरित कर दिया है। यह कसावट कहानीकार की इसी कला का द्योतक है। इस कहानी में वह औरत, जो देखने में ’बुरी भी नहीं’ थी, जब गोरेसाँवले युवकों में से गोरे से यह कहती है कि ’’मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती’’, तब उसका यह कथन अपना अर्थविस्तार करता हुआ पूरी कहानी पर छा जाता है। इस कहानी के नामीगिरामी आलोचकों को भी गोरे ओर साँवले की बातचीत समझ में नहीं आ पाती है। फर्क इतना ही है कि वह सीधीसादी सरल दीखने वाली औरत खुले दिल से इसे स्वीकार कर लेती है। पर कहानी के आलोचक इस कहानी के वार्तालाप को आदि से अन्त तक पढ़सुनकर भी इसे न तो समझ पाते हैं और न इसको वे स्वीकारना ही चाहते हैं। यहाँ वे ऐसीऐसी टिप्पणियां करने लग जाते है, मानो उनसे अधिक इस कहानी को समझने वाला और कोई है ही नहीं। दूसरी ओर जब उन्नत और पुष्ट उरोज’ वाली वह औरत अपना देहव्यापार कर लेने के बाद गोरे से अपनी कमाई के रुपये देने की बात करते हुए मोलतोल करती है और सामान्य रकम से दोगुनी रकम- दोदो रुपयों की जगह आज चारचार रुपये लेने की बात करती है तब वह केवल आठआठ आने और देने की बात कर उसके डिमांड पर ताला लगा देता है और दस रुपयों का नोट भुनाने के बहाने पास की चाय की दूकान की ओर चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही दोनो अपनेअपने जूते अपनेअपने हाथों में लेकर अरबी घोड़ो की तरह भाग खड़े होते हैं- ’’तब उस औरत को शायद गोरे की बात समझ में आती है और वह अपनी छाती पीटपीछ कर विलाप करने लगती है- अरे लूट लिया रे, हरामी बच्चों ने। उनपर बज्जर गिरे- तब कहानी के पाठकों को यह बात समझ में आने लग जाती है कि इस देश की जनता बारबार उस औरत की तरह क्यों लूट ली जाती है, अपने आश्वासनों के बावजूद आज़ाद देश के लूटेरों से? वह गोरे और साँवले- पूँजीपतियों और वामपथियों- दोनो के द्वारा लूट ली जाती है और जो कोई इस लूट से उसे बचाने आगे आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए यह गोपन देहव्यापार करने वाली औरत के लूट लिये जाने की कहानीमात्र नहीं है, बल्कि देश की जनता को भी इसी तरह, वोट का उपयोग करने और जनता को लूटने वाले गोरेकाले की कहानी भी है। यहाँ प्रतिरोध करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाने वालों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस तरह कहानी बहुत दूर तक अपनी इस अर्थगूँज को मुखर कर जाती है।
इस कहानी को पढ़ने के साथ ही मेरे मन में सहसा जो प्रश्न उठा था कि इस कहानी में वास्तव में ये ’हत्यारे’ कौन हैं, यह प्रश्न अपना उत्तर माँगता है। क्या केवल गोरा ही, जैसा इस कहानी की पृष्ठभूमि में लगता है, हत्यारा है? काला न तो हत्यारा है और न ही हत्या की साजिश में शरीक ही है। यह तो अचानक की गयी हत्या है, जिसके लिए गोरे में उसकी मानसिकता पहले से बनी हुई है। जब मैंने यह सोचना और कहानी में झाँकना शुरू किया कि आखिर ये हत्यारे कौन लोग हैं और ये हत्या किसकी करते हैं, तो उत्तर अपनेआप मिलने लगे कि आखिर आज़ाद भारत में हत्यारा कौन नहीं हैं? सूची लम्बी होती गयी- नेतागण मंत्री, प्रशासक, शिक्षाविद् अध्यापक, अभियन्ता, तथाकथित समाजसेवी आदिआदि। प्रश्न यह भी कि हत्या किसकिसकी नहीं होती है? हत्या तो हो चुकी है- नैतिकता की, ईमानदारी की, भाईचारे की, मानवता की इंसानियत की और कुल मिलाकर देश के ’लोकतंत्र’ की। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसके मूल में एकमात्र कारण ’अर्थ’ है ’मनी’ है, रुपया है। इसको लूटनेखसोटने, घोटाला करने, ग्रैविग करने, समांतर कालाधन का विस्तार करने, मुद्राव्यापार का समांतर संसार खड़ा करने और अपनाअपना घर भरने के लिए दिनदिहाड़े की जाने वाली हत्याएँ हैं यहाँ। इसीलिए यह भारत के पूरे लोकतंत्र की हत्या है। हम ’फाउल डेमोक्रैसी’ से अराजक ;।दंतबीपब क्मउवबतंबलद्ध में जी रहे हैं। यह फेज़ लोकतंत्र की हत्या के बाद का फेज़ है। यहाँ अनुशासन, आत्मानुशासन कर्मसंस्कृति सबकी हत्या हो चुकी है। इसीलिए यहाँ हत्यारे और हत्या के कारण का अर्थविस्तार दिखाई पड़ता है।
’हत्यारे’ कहानी के दोनों पात्र- गोरे और साँवले- शिक्षित वर्ग से आते हैं। इनकी बातचीत सुनने में अवसंगतविसंगत या एब्सर्ड लगती है। ’अविश्वसनीयता’ इसकी विशेषता है। भाषा व्यवहार शास्त्रीय Pragmatic चिन्तक ग्राइस Grice ने अपने विवक्षासिद्धांत Theory of Implicature में गुणसूत्र Maxim of Quality के खंडन की बात की है। गोरे और साँवले की आंरभिक बातचीत में कहीं भी विश्वसनीयता नहीं है। उसे न तो सत्यापित Verify किया जा सकता है और न उसे सत्य माना जा सकता है। पर इनका वार्तालाप अपनेआप में गू़ढ़ार्थ को छिपाए हुए है। गोरा साँवले से कहता है- यही नेहरू है, यार! आज उसका एक और पत्र मिला है। हाँ, डियर यह आदमी मुझको परेशान कर रहा है। मैंने बारबार कहा कि भाई मेरे भारत की प्राइममिनिस्टरी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो। मेरे पास बड़ेबड़े काम हैं। लेकिन मानता ही नहीं। वही पुराना राग। इस बार लिखा है- अब मैं थक गया हूँ। गाँधी जी देश का जो भार मुझे सौंप गये उसको मैं आपके मजबूत कंधों पर रखना चाहता हूँ। इस अभागे देश में आज आपसे काबिल और समझदार दूसरा कोई भी नहीं है। नेहरू देश के सभी नेताओं को निकम्मा और बातूनी समझता है। तुमको तो मालूम है कि लास्ट टाइम मैं जब दिल्ली गया था तो नेहरू ने अशोक होटल में आकर मुझसे मुलाकात की थी….’’ नेहरू हाथ पकड़ कर रोने लगा। बोला- आज देश भारी संकट से गुजरा रहा है। सभी नेता और मंत्री बेईमान और संकीर्ण विचारों के हैं। जो ईमानदार हैं, उसके पास अपना दिमाग नहीं है। मेरी लीडरशिप भी कमजोर है। मेरे अफसर मुझ को धोखा देते हैं। जनता की भलाई के लिए मैंने पांचसाला योजनाएँ शुरू कीं, लेकिन ब्लौकों के सरकारी कर्मचारी अपने घरों को भरने में लगे हैं। मैं जानता हूँ कि सारे देश में कुछ लोग लूटखसोट मचाये हुए हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर सकता। देश को आज केवल आपका ही सहारा है। आप ही पूँजीपतियों, मंत्रियों और अफसरों के षड्यंत्र को खत्म करके समाजवाद कायम कर सकते हैं।’’ यह सारा वाकया सुनकर साँवला गोरे से पूछता है- तब तुम क्या सोच रहे हो? गोरा बताता है- ऐसे छोटेमोटे काम माबदौलत नहीं करते। पर जब सांवला उससे थोड़ा झुकने के लिए कहता है तब गोरा जवाब देता है- ’’नहीं’ बे, मैं सिद्धांत का आदमी हूँ। नेहरू को ट्रंक काल करके आ रहा हूँ। इसीलिए तो देर हुई। हाँ, मैंने साफसाफ कह दिया कि देश की प्राइम मिनिस्ट्री मुझे मंजूर नहीं। मेरे सामने बहुत बड़ेबड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे विश्वशान्ति स्थापित करनी है।’’ यहाँ कथाकार के द्वारा कहानी में लाया गया गोरे और नेहरू की बातचीत का सन्दर्भ कोई दिवास्वप्न नहीं है। यह कोई स्वैरकल्पना या समाजराजनीतिक फंतासी भी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कथाशिल्प है, जो घटितव्य Ought to be को घटित happened के रूप में उजागर कर देता है। यानी यही सही समय था जब नेहरू को प्रधानमंत्रित्व से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1962 में ही देश चीन से हुए युद्ध में हार गया था। यही नहीं, अपने देश की काम्य अभीष्ट लोकतंत्रिक व्यवस्था दम तोड़ चुकी थी और वह आलोकतांत्रिकता की ओर मुड़ गयी थी। एक श्ूतवदह प्दकपंश् उभर कर आ खड़ा हुआ था। देश एक ऐसे मोड़ पर आगे बढ़ पड़ा था, जहाँ गलत भारत का प्रतिनिधि बन कर एक अवांछित वर्ग उभर कर सामने आ चुका था। कहानी के दोनो पात्र इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीति का अपराधीकरण धुआँधार बढ़ चुका था। नेताओं और मंत्रियों में बेईमानी और विचारों की संकीर्णता जड़ बना चुकी थी। सारे देश में लूटखसोट का बाज़ार गर्म था। अफसर धोखेबाज थे। वे षड्यंत्रकारी हो चुके थे। वे अपनाअपना घर भरने में दिनरात लगे हुए थे। आज़ादी के केवल पन्द्रह वर्षों के भीतर गाँधी के रामराज्य को स्थापित करने का उद्देश्य लेकर चलने वाला लोकतंत्र नष्ट हो चुका था। नेहरू इसी ’राँग इंडिया’ वाले वर्ग के दो युवकों में से एक को अपना प्रधानमंत्रित्व सौपना चाहते थे। यानी वह रांग इंडिया से बाहर नहीं निकल पाये थे। इस करुणापूर्ण विलाप करने वाली स्थिति में प्रधानमंत्री का ताज और अपने परिवार के अतिरिक्त किसी और के सिर पर रखना नहीं चाहते थे।
नेहरू के बाद शास्त्री, शास्त्री के बाद इन्दिरा और इंदिरा के बाद राजीव- इसी नामितीकरण के उदाहरण और प्रमाण है। इस बिन्दु तक आतेआते भारतीय लोकतंत्र की हत्या हो चुकी होती है। लूटखसोट कर अपनाअपना घर भरने वाले नेता, मंत्री, अफसर भारतीय लोकतंत्र के हत्यारे सिद्ध होते हैं। उन्होंने पंचशील के कबूतर उड़ाये थे, हिन्दीचीनी भाईभाई का नारा लगाया था। लोकतंत्र की हत्या का एक बड़ा कारण नेहरू स्वयं भी हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को कर्मसंस्कृति को सही दिशा में नेतृत्व या नायकत्व नहीं किया और वह निरन्तर अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेज़ियत की राजतंत्रीय मानसिकता में डूबे रहे। उनकी इस विफलता के मूल में उनकी विश्वशान्ति की ललक और देश से अधिक विदेश के प्रति सम्मोहन, आकर्षण और निजी महत्त्वाकांक्षा की अधिमानता के आगे देश में घट रही घटनाओं के प्रति और कर्तव्यपरायणता के प्रति उनकी निष्क्रिय विमुखता भी एक बड़ा कारण बनी। वह लोकतंत्र में लगे रोग को तो पहचान गये थे ।पर न तो उससे वह बचाव कर सकते थे और न ही उसका सही निदान दे सकते थे।
कहानी में नेहरू गोरा से कहते है कि मैं किसी गांधीवादी के मजबूत कधों पर प्राइममिनिस्ट्री का दायित्व देना चाहता हूँ और तुम्हीं मेरी दृष्टि में इसके लिए सर्वाधिक योग्य हो। अतः तुम इस दायित्व को स्वीकार कर लो। पर यहाँ भी नेतृत्व ’रांग इंडिया’ का दिया जा रहा है। वास्तव में नेहरू को अपनी विफलता में उसी समय किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को अपने सामने ही प्रधानमंत्री बनाने की त्यागमयी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी। यहाँ कहानी में जो कथित है, वह वास्तविकता में अकथित है। ऐसा नहीं हो पाया।
गोरे और नेहरू के इस बातचीत के समांतर साँवला अमेरिका के प्रेजिडेंट केनेडी के द्वारा उनकी प्रेजिडेंटशिप के सौंपे जाने की बात करता है। पर वह भी इसके लिए तैयार नहीं हो पाता है। पर यहाँ केनेडी की बातचीत से इतना तो उद्घाटित हो ही जाता है कि अमेरिका भावी विश्व युद्ध की स्थिति में रूस पर विजय प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह भारत का उपयोग या इस्तेमाल करना चाहता है।
अवांछित भारत Wrong India के ये दोनों गोरे और सांवले पात्र और इनकी मनोवृत्ति जिस शैक्षणिक परिवेश की उपज हैं, कहानीकार इस पर भी प्रकाश डालता है और यह भी इन दोनों पात्रों की बातचीत के व्याज से ही। पर यहाँ शिक्षा की जिस पतित निकृष्ट स्थिति को उद्घाटित किया गया है, वह तो ’अवांछित भारत’ का एक अनुभागमात्र है। यहाँ ऐसे अनगिनत क्षेत्रों और अनुभागों की ओर संकेत जाता है- वे क्षेत्र राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सचिवालयों, अभियंताओं, चिकित्सकों, समाज, राजनीति, अर्थतंत्र- सभी क्षेत्रों की ऐसी ही भ्रष्टता, बेईमानी और घूसखोरी की घृण्य स्थितियाँ संकेतित होती हैं। नेहरू जिस ’अवांछित भारत’ को देखकर निराशा से भर उठे थे, उस अवांछित भारत को जन्म देने और उसे विकसित करने में स्वयं नेहरू का ही योगदान रहा था। पर समय रहते उन्हें इसका बोध नहीं हो पाया। गोरे के सामने नेहरू के रो उठने का यही कारण है। राममनोहर लोहिया याद आते हैं। उन्होंने चरित्र निर्माण की बात कही थी। भारत में नेहरू से अब तक इस दिशाहीन चरित्र का तो क्षरण और लोप होता चला गया है। नेहरू में स्वयं के लिए तो कर्मसंस्कृति थी। पर यह कर्मसंस्कृति और अनुशासनात्मकता न तो वह अपने मंत्रियों, सांसदों और नागरिकों को दे सके, जिसके बल पर लोकतंत्र उन्नत हो सका होता। दूसरे, उन्हें देश की, अपने मंत्रालय की वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। उनमें उद्देश्य को चरितार्थ और प्रतिपादित करने वाली कर्मसंकल्पता नहीं थी। लोहिया ने 1962 में उनके उस कथन की याद अपने श्रोताओं को करायी थी जहाँ उन्होंने अपनी पलटन (सेना) से कहा था कि चीनियों को बार्डर से भगा दो, उन्हें खदेड़ दो। पर क्या इसके लिए इस दिशा में उन्होंने कर्मनिष्ठता दिखाई थी? केवल फाइलों को डिस्पोजऑफ़ करने में सच्ची कर्मनिष्ठता नहीं होती, वह उन सारे दायित्वों के प्रति होती है, जिनकी ओर न उनमें दिशाबोध था और न ही अपेक्षा को साकार करने की, सारी तैयारी को समय से मुकम्मल करने का कभी कोई प्रयास ही किया गया था और न ही ऐसा कोई उद्यम था। सरकार का हर उद्यम घाटे का सौदा बनने लगा था। लोग उससे अपनाअपना घर भरने लगे थे। मूल समस्या कामचोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, समांतर आर्थिक सरकार चलाने और राजनीति का अपराधीकरण करने- माफियागिरी पैदा हो जाने की थी। नेहरू लोगों को अपना जीवनस्तर ऊँचा करने की बात करते थे और जो ऐसा करता था, उसे देखकर वह प्रसन्न होते थे। पर यह सबकुछ होता कैसे था, उस ओर उनकी दृष्टि नहीं जा पाती थी। इन्हीं सबने ’अवांछित भारत’ Wrong India को जन्म दिया था। कहानी के दोनों गोरे और साँवले पात्र- इसी अवांछित भारत का आत्मिक और बाह्य निरूपण करते है। वे मुफ्तखोरी, ऐशमज़े करने वाले, लूटखसोट करने वाले, गरीब नारियों का यौनशोषण करने वाले छात्र नागरिक है। उनके कथनों पर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये रचनात्मक कार्य करने चल पड़े हैं। उनमें गोरा कहता है- ’’आज समय आ गया है कि हमारे युवक बुद्धिमानी, मौलिकता, साहस और कर्मठता का परिचय दें। मैं पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से उनका पथप्रदर्शन करना चाहता हूँ। ’’काला इससे आगे बढ़कर कहता है कि आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति करने का समय आ गया है।’’ वे दोनो मजे करते हैं नारी का देह भोगकर उसे रुपये न देकर झांस पट्टी देकर भाग खड़े होते हैं। इधर इन्हें पकड़ने के लिए जो युवक दौड़कर इनका पीछा करते हैं, उनमें से एक को अब अपने बहुत निकट पाकर कि कहीं वह साँवले को पकड़ न ले, वह उसको छुरा मार देता है। उसकी तत्काल हत्या हो जाती है। नैतिकता शर्मसार हो उठती है। इस कहानी में एक नहीं ऐसी अनेक हत्यारें अन्तर्गर्भित है। इसी अवांछित भारत के कारण नेहरू अपनी प्राइममिनिस्ट्री छोड़ना चाहते है। पर क्या सचमुच ऐसा था। यहाँ मंत्री हत्यारे हैं। अफसर हत्यारे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर- सभी हत्यारे हैं। प्रोफे़सर ने शिक्षा को अपने जीवन का केन्द्र नहीं बनाकर काम ;ैमगद्ध और ’काला धन’ (ब्लैकमनी) के लिए शिक्षा को इसका माध्यम बना रखा है। यह अपने छात्रों से किताबें लिखवाता है और उसे अपने नाम से छापता है। जिस छात्रा पर उसकी नज़र पड़ती है, उसे यह अपने जाल मे फँसा कर हड़प लेना चाहता है। हत्यारे में नैतिकता की हत्या होती है। इस कहानी में विभिन्न क्षेत्रों में लोकतंत्र की हत्या के कारण अवांछित भारत ही शेष रह जाता है। लोकतंत्र की हत्या कर दिये जाने के बाद आखिर शेष क्या बचता है? बचता है छोटेछोटे राजतंत्रीय सामन्ती केन्द्र, स्वार्थ से प्रमत्त अधिकारों के शोषक केन्द्र। खुदगर्ज़ अराजक भीड़तंत्र। इसीलिए गोरे और साँवले दोनों लोकतंत्र विहिन अँधेरे में खो जाते है।
अमरकान्त का पहला कहानीसंग्रह ’समकाल की कहानियाँ’ नाम से 1958 ई. में इलाहाबाद के 2 मिंटो रोड़, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इसमें उनकी पहली कहानी ’डिप्टी क्लकटरी’ है और अंतिम कहानी ’ज़िन्दगी और जोंक है। जिस लोकतंत्र में हमारे नवयुवक लुटेरे और हत्यारे हो, जाते है इनका भविष्य क्या होगा? वह अंधकार से भरा नहीं होगा, तो भला और क्या होगा? इस युग में आरंभ में ही राजनीतिक अपराधीकरण हो चुका था। पर अब तो समाज का भी अपराधीकरण हो चुका है और अब यह अपराध केवल अवांछित भारत Wrong India निर्मित करने वाले वर्ग तक सीमित नहीं रहा है। लोकतंत्र की हत्या के बाद अब केवल अराजक तंत्र शेष रह गया है।
अमरकान्त गाँधीवादी थे, वह नेहरू को बेहद पसन्द करते थे। पर 1962 तक आतेआते नेहरू के प्रति उनका मोहभंग हो चुका था। लोकतन्त्र की लूटखसोट और हत्या से उत्पन्न भयावह स्थिति उनकी आँखों के सामने थी। अवांछित भारत का नग्न दृश्य केवल उनकी आँखों के सामने नहीं था, बल्कि उनके मनमस्तिष्क में छाया हुआ था। उनकी लेखनी ने इसकी बहुत साभिनप्राय अभिव्यक्ति हुई है। अमरकान्त को पता था कि कहानी में कितना कहना जायज है और इसकी हद को तोड़ देना नाजायज है। उनकी अपनी इस कहानी में कथ्य कसा हुआ है, वह नाभिकेन्द्रिक है। इसके लिए उन्होंने अपनी अद्भुत भाषाक्षमता का प्रमाण उपस्थित कर दिखाया है। भाषाव्यवहार का इतना कुशल व्यवहार या कहूँ कि भाषाव्यवहार के व्याकरण का इतना वर्गगत सार्थक और सटीक उपयोग हिन्दी कहानी में – 1962 से 2022 तक देखने को और कहीं नहीं मिल पाता है।
1962 में कहानीकार ने जिस अवांछित भारत की दिशा और सूरत हमें दिखा दी थी, आज का भारत इक्कीसवीं सदी से आगे सारे बंधन तोड़कर आगे निकल चुका है। अब केवल इस सर्वव्यापी पतन का जिम्मेदार हत्यारा वह युवावर्ग नहीं रह गया है, बल्कि अपनेअपने स्तर और स्तृतियों में परे उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम साथ ही मध्यम और निम्न से निम्नतर वर्ग तक इसकी सक्रियता परिव्याप्त हो चुकी है।

पाण्डेय शशिभूषण ‘शीतांशु’
जन्म : 13 मई, 1941
शिक्षा : पीएच. डी. (हिन्दी), डी. लिट्. (भाषा-विज्ञान), स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अनुवाद)।
गतिविधियाँ : हिन्दी में वादमुक्त आलोचना के शिखर-पुरुष तथा सुप्रतिष्ठ सैद्धान्तिक और सर्जनात्मक आलोचक। जितनी व्यापकता और गहनता में प्रतिमानों की दृष्टि से भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना-सिद्धान्तों की शक्ति-सीमा पर मौलिक चिन्तन-मनन किया, उतनी ही सूक्ष्मता और प्रातिभ अन्तर्दृष्टि से हिन्दी में पहली बार कुछ प्रसिद्ध साहित्य-पाठों (कविताओं, उपन्यासों, कहानियों और नाटकों) की सार्थकता और साभिप्रायता का तलोन्मेषी उद्घाटन भी किया है।
ये एक निर्भीक प्रत्यालोचक भी हैं। इन्होंने पन्त, दिनकर, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आदि शीर्ष साहित्यकारों द्वारा स्थापित-प्रचारित प्रत्येक भ्रान्त मतवाद का युक्तियुक्त निरसन एवं निर्मूलन किया है। साथ ही अपना प्रमाणपुष्ट प्रतिपादन भी प्रस्तुत किया है।
साहित्य-सेवा : 40 पुस्तकें तथा 350 से अधिक शोधालेख प्रकाशित।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर से अवकाश-प्राप्त (1977-2001) प्रोफ़ेसर। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (अक्तूबर 1988), महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (जनवरी 2005-दिसम्बर 2007) तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद (फरवरी एवं नवम्बर 2009) में विजिटिंग प्रोफ़ेसर रहे। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 1991 में त्रिनिदाद एवं 1995 में पेइचिंग विश्वविद्यालय के लिए विजिटिंग प्रोफ़ेसर नियुक्त। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा से प्रकाशित ‘तुलनात्मक साहित्य विश्वकोश’ (2008) का प्रविष्टि-लेखन करवाया एवं अतिथि-सम्पादन किया।
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा 2020 के ‘भारत भारती सम्मान’ से सम्मानित।
Discover more from रचना समय
Subscribe to get the latest posts sent to your email.